 |
| देव प्रकाश चौधरी |
बिहार और झारखंड का सांस्कृतिक चेहरा इतना काला और डरावना शायद पहले कभी नहीं रहा। हाशिये से भी बाहर हो गई है संस्कृति....लेकिन फिर भी उम्मीद बची हुई है। उम्मीद है तो ही जीवन है और जिस दिन यो उम्मीद ध्वस्त हो जाएगी, फिर न तो किसी के कूकने से भी नहीं लौटेगा बसंत और न ही किसी के बोलने से नहीं पाहुन।
व्यवस्थित और शिक्षित माने जाने वाले उस गांव में आगंतुकों की कतार थमने का नाम ही नहीं ले रही। मानो गोड्डा जिले के मोतिया गांव की आबादी अचानक बढ़ गई हो। सिनेमा का गाना नहीं, झूमर और लोकगीत! बरसों बाद विशेषर शर्मा आया है। बेजोड़ गाता है......... बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल! क्या गला पाया है? गंजेड़ी है तो क्या हुआ? गुणी आदमी है। ढोलकिया भी खूब ताल देता है........ सब तरफ यही चर्चा। पड़ोस के गांव की औरतें भी दल बांध कर आ रही हैं। पढ़ी-लिखी औरतें भी हैं और ऐसे लोग भी, जो टीवी के आदी हो चुके हैं।लोकधुन की बयार में रात भर सैकड़ों लोग बहते रहे और कब सुबह हो गई, पता नहीं चला। बात बहुत पुरानी नहीं है और तब के बिहार की है,जब झारखंड भी बिहार का हिस्सा था।
आज किसी को नहीं पता, रात भर लोगों को रिझाने वाले लोकगायक विशेषर शर्मा कहां हैं? किस हाल में हैं? तेजी से भाग रही जिंदगी में शायद किसी को इस जानकारी की जरूरत भी नहीं। क्योंकि बदलते वक्त ने बिहार की सांस्कृतिक अस्मिता को उस फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां लोक संस्कृति के लिए पैर रखने की भी जगह नहीं। देखते-देखते हाशिये से भी बाहर हो गए लोक कलाकार, बेरंग हो गई लोककला।
तकनीकी विस्फोट और साधनों के लोकतंत्रीकरण ने मनोरंजन के नए मुहावरे गढ़े हैं और लोगों की हथेली में सिमट चुकी इस दुनिया के शोर में उस जट की आवाज भी कहीं गुम हो गई है, जो कहता था- हम लाया आजन-बाजन तुम करो बियाह। हाल के दिनों में किसी ने नहीं देखा, जटिन को मनुहार करते हुए- जब-जब टिकवा मांगलियो रे जटवा, टिकवा काहे न लऔले रे। याद है आपको आपने कब गंगा किनारे अपने नाव पर लेटे-लेटे किसी मांझी को गाते हुए सुना है- दूर कछार सजनी का यार। शायद आपने किसी भगतिया को मृदंग के साथ भटकते हुए भी नहीं देखा होगा, लेकिन कभी उनका भी जमाना था।
सच है कि दिल बहलाव के उपकरणों और कल्पनाशील आयोजनों से मनोरंजन की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। कहा जाए तो अब मनोरंजन के साधनों का भी लोकतंत्रीकरण हो चुका है। बिहार और झारखंड भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे में लोककलाकारों के लिए सबसे बड़ी चूनौती है...... अपने लिए दर्शक और श्रोता तैयार करना।
कभी बिहार में धनकटनी, नृत्य और गीत के बिना पूरी नहीं होती थी। जब भी कोई किसान अपना नया गुहाल (गौशाला) बनाता था, एक खास किस्म के नृत्य लोढ़ियारी का आयोजन होता था। इस नृत्य का नायक किसान होता था और उसके गीतों में मवेशियों के प्रति एक सम्मान की भावना झलकती थी। आज लोढ़ियारी नृत्य बिहार के सांस्कृतिक शब्दकोश से भी बाहर हो गया है। यही हाल मछली बेचने का स्वांग रचने वाली नृत्य विधा गोढ़िन, छोटे-छोटो बच्चों के नृत्य घो-घो रानी, गंगा के किनारे होने वाले गांगिया, प्यार को लौकिक विश्वास की कसौटी पर परखने वाली नृत्य शैली बगुलो और देवताओं को समर्पित देवहर का है। नाच की शैली झरणी और बसंती भी कहीं खो गई है। हालांकि उम्मीद अब भी बची हुई है। बिहार के युवा शास्त्रीय गायक अजय राय जब बिहार की सांस्कृतिक अस्मिता की बात करते हैं , तो वह बहुत निराश नहीं दिखते- "क्योंकि लोक धुनें दर्शकों की भावना को साथ लेकर जीती हैं और साथ ही मरती हैं, इसलिए ये संकट बहुत जल्दी छंट जाएगा।"
कारू महरा भी हताश नहीं नजर आते। पंचकौड़ी मृदंगिया की तरह झारखंड के गोड्डा जिले के मोतिया गांव के भगतिया कारू महरा को भी एक नटुआ की तलाश है। अमर कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया का नायक पंचकौड़ी एक भगतिया ही था, जो मृदंग बजाता था और अपने दल का मूलगैन था। उसे एक नटुआ की तलाश थी ताकि एक बार फिर से उसका दल जीवित हो सके और एक बार फिर से सुर, लय और ताल की त्रिवेणी में भगतिया का भाग्य चमके। कारू महरा की उम्मीद अभी बनी हुई है। यह जानते हुए भी कि अब गांव के लोगों की रुचि इस तरह के नाच-गानों में बहुत नहीं रह गई है। कारू कहते हैं- "कुछ भी हो जाए, जिस दिन सुर और लय से जिंदगी अलग होगी, सबी असुर कहलाएंगे।" भगताय गाने वाले हर हाल में रहेंगे, क्योंकि गायन की यह परंपरा लोक विश्वास पर टिकी है। यही विश्वास है कि तमाम संकटों के बावजूद लोक की उष्मा बची हुई है। यही भरोसा है कि भागलपुर की चक्रवर्ती देवी बिना किसी अपेक्षा के यहां तक कि लोगों की उपेक्षा से बचते हुए मंजूषा कला में रंग भरती रही हैं.......... नहीं तो कई दशक पहले बिहार की यह लोककला किसी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही होती। लोक संस्कृति की उष्मा और इसकी ताकत देखनी हो तो मैं आपको थो़ड़ी देर के लिए बिहार से राजस्थान ले जाने की अनुमति चाहूंगा।
हांजी रे दीवारा थारा डेरा लद्या जाय........ कुछ यही तो गाया था राजस्थान के लंगा कलाकारों ने और ढोलक, खड़ताल, अलगोजा, सारंगी और मोरचंग की लयबद्ध और उत्तेजक संगीत लहरियों पर सुरक्षा घेरे की परवाह किए बगैर झूम पड़े थे प्रिंस चार्ल्स। भाषा की दीवार का कोई अर्थ नहीं रह गया था और जमाना अचंभे में पड़ गया था। पारंपरिक लोक अनुरंजन के माध्यमों की कुछ विशेषता ही ऐसी है कि वे अजनबी को भी तुरंत और सदा के लिए अपना बना लेते हैं।
लेकिन बिहार और झारखंड की नई पीढ़ी को आखिर हो क्या गया है? यह सवाल कुछ दिन पहले ट्रेन पर बिहार के एक सारंगी बाबा श्याम सुंदर गोस्वामी ने पूछा था। गली में नौ मन के अजगर का शोर करते हुए बाइस्कोप आता है तो कोई बच्चा मां का आंचल पकड़ कर बाहर चलने की जिद नहीं करता। गोस्वामी की चिंता यह थी कि लोग भीख तो दे देते हैं, लेकिन कोई सारंगी सुनना नहीं चाहता। आज की नई पीढ़ी सारंगी के सुरों के साथ गोरखनाथ की कथा नहीं सुनना चाहता। आप मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों के पास जाएं, कुछ यही दर्द है उनका।
सामा-चकेवा के मौके पर कोई तू-तू मैं-मैं नहीं होती। कुएं के पास जाकर कोई पनिहारिन कोयला माय के लिए रसोईघर में जगह नहीं। गली में नौ मन के अजगर का शोर करते हुए बाइस्कोप आता है तो कोई बच्चा मां का आंचल पकड़ कर बाहर चलने की जिद नहीं करता।
क्या यह एक सांस्कृतिक संकट नहीं है। खासकर बिहार और झारखंड जैसे प्रदेश के लिए, जहां की जिंदगी सदियों से लोक से उष्मा लेती रही है। शायद इसका जवाब हमें खुद ढूंढना होगा, कहते हैं बिहार के वरिष्ठ कलाकार और संस्कृतिकर्मी कपिलदेव राय। आज हमने खुद को लोक संस्कृति से अलग करने की होड़ में शामिल कर लिया है। लोक अनुरंजन में कभी ऐसा नहीं होता था कि गाने-वाले कोई और हों और सुनने वाले कोई और, रचनेवाले कोई और हों और देखनेवाले कोई और। जब तक लोक कलाकार हमारे बीच से खड़ा नहीं होगा, यह संकट बढ़ता जाएगा, क्योंकि तेजी से बदल ली है हमने अपने जीने की आदतें। राय की आवाज में लोक सोस्कृति के इस संकट का दर्द साफ महसूस किया जा सकता है।
सच है कि आज देश का मनोरंजन उद्योग 20,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। विज्ञापन की बढ़ती पहुंच आमोद-प्रमोद के तौर-तरीके, सोच और शैली बदलने में लगी है। बड़ी कंपनियां अपने साधनों में इस बात की वकालत करती दिखती हैं कि मनोरंजन सार्वजनिक न हो कर व्यक्तिगत चीज है। उनके लिए ग्राहक ही रसिक है और वही सच्चा कला पारखी। इंटरनेट ने तो दुनिया का भूगोल ही छोटा कर दिया गै, एफएम के नए तेवर के साथ रेडियो के बीते दिन लौट आए हैं। चैनलों की बढ़ती संख्या ने पश्चिम की जीवनशैली के प्रति लोगों का मोह बढ़ाया है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारे आमोद-प्रमोद के पुराने और परंपरागत तरीके जिंदगी से बाहर हो गए हैं। भागलपुर, पटना, दरभंगा, रांची, बोकारो, गोड्डा, दुमका और मुजफ्फरपुर की दुकानों में मेडोना और माइकल जैक्सन के सम्मोहन से मुक्त लोग बालेसर का गाया-घोड़ली पर चमके पिया की पगड़िया सेजिया पर बिंदिया तोहार हो- जैसे गीतों को खोजने आ ही जाते हैं। पिया की जो छवि बालेसर सजाते थे, उसे कोई भी कृतज्ञ समाज कैसे भूल सकता है। तभी तो समाम संकट के बावजूद उम्मीद बची हुई है। ऐसे में शहंशाह आलम की इन पंक्तियों को याद करना जरूरी है-
जब तक एक भी कुम्हार है
इस धरती पर
और
मिट्टी आकार ले रही है
समझो कि
मंगलकामनाएं की जा रही हैं।
उम्मीद है तो ही जीवन है। और जिस दिन यो उम्मीद ध्वस्त हो जाएगी, फिर न तो किसी के कूकने से भी नहीं लौटेगा बसंत और न ही किसी के बोलने से नहीं पाहुन।
-देव प्रकाश चौधरी
परिचय-
मूलत चित्रकार, लेकिन पेशे से पत्रकार। देश और विदेश की कई महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी। पत्र-पत्रिकाओं में दो हजार से ज्यादा लेख प्रकाशित। बिहार की मंजूषा कला पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से फैलोशिप। इसी विषय पर किताब, लुभाता इतिहास, पुकारती कला किताब, प्रकाशित और बेहद चर्चित। 1000 से ज्यादा साहित्यिक पुस्तकों के कवर डिजायन किए। फिल्मों के लिए लेखन, वृतचित्रों का निर्माण। प्रिंट और टीवी में सामान्य रूप से सक्रिय। इन दिनों एक फीचर फिल्म के संवाद लेखन में व्यस्त, साथ में पत्रकारिता की नौकरी भी।
संपर्क-deop.choudhary@gmail.com


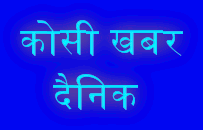







































3 टिप्पणियां:
Basundhara: Devprakash choudhri ka aalekh kavya ki bhasa men likha gaya man ko bha gaya. Sachmuch men visesar ji aur baleswar ji ko yah angpredes kabhi nahi bhul sakta.
बेटा भेल लोकी लेल बेटी भेल फेकी देल! क्या गला पाया है? गंजेड़ी है तो क्या हुआ? गुणी आदमी है। आपने बिहार-झारखंड के जीवन्त यथार्थ को उकेरा है , यह सच है ...और यही सच है, जिसे आपने लिखा है !
dil se kahu aapne bahut zaruri baat kitaraf ishara kiyaa hai. is aalekh ko ham apani maati par saajhaa kar rahe hain.
एक टिप्पणी भेजें